मुक्ति भवन
मुक्ति भवन
ओशो ने “मैं मृत्यु सिखाता हूँ” पुस्तक में कहा है , “जन्म और मृत्यु में गुण का फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ मात्रा का फ़र्क है। ये विलोम शब्द नहीं है। जन्म बढ़ते-बढ़ते मृत्यु बन जाती है। इसका मतलब ये कि जन्म और मृत्यु एक ही चीज़ के दो बिन्दु हैं।
न जाने कैसी नासमझी में, न मालूम किस दुर्दिन में आदमी को यह ख़्याल बैठ गया कि जन्म और मृत्यु में विरोध है। हम जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। और हमें यह पता नहीं है कि हमारे जीने में ही मरना छिपा ही है। और जब हमने एक बार तय कर लिया कि हम मरना नहीं चाहते, तो उसी वक़्त तय हो गया कि हमारा जीना भी कठिन हो जाएगा।”
मृत्यु, मृत्यु की प्रक्रिया की शुरुआत, और मृत्यु का स्वीकार्य- बेहद गूढ़ और जटिल विषय है। अनेक महापुरुषों ने व्याख्या की लेकिन तब भी हम जीवन और मृत्यु को एक ही चीज़ के दो सिरे मान पाने में असमर्थ होते हैं। मृत्यु क्यों, और मृत्यु के बाद क्या, मुक्ति, मोक्ष इन सारी बातों के बारे में तो कल्पना और विवाद किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु के बारे में एक बात तयशुदा रूप से कही जा सकती है। वह यह कि इस प्रक्रिया का प्रभाव मृत्यु पाने वाले से कहीं ज़्यादा मृत व्यक्ति के आसपास के लोगों पर पड़ता है। याने कि मृत्यु का सबसे बड़ा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। सुभाशीष भूटियानी की “मुक्ति भवन” इसी प्रभाव को हमें दिखाने की एक कारगर कोशिश है।
एक अजीब कहानी और दुखद विषय से निबाह करने वाली ये फ़िल्म बहुत ही रोचक और दर्शनीय है। कहानी कुछ यूं है कि, वयोवृद्ध रिटायर्ड स्कूल मास्टर दयाशंकर एक दिन महसूस करते हैं कि उनका अंत निकट है और अब बनारस में अपने जीवन के अंतिम दिन बिता कर संसार से विदा लेना चाहते हैं। उनका मुक्ति-भवन नामक एक होटल में अपने पुत्र के साथ आखिर के कुछ दिन बिताना, और इस बीच उनके और उनके बेटे के बीच के रिश्तों में आने वाले उतार चड़ाव, इस कहानी का मर्म है।
“मुक्ति भवन” फ़िल्म की कहानी और पटकथा लिखी है सुभाशीष भूटियानी और असद हुसैन ने और इसे निर्देशित भी स्वयं सुभाशीष भूटियानी ने ही किया है। ये मात्र 21 वर्ष के उम्र में सुभाशीष की प्रथम निर्देशित फ़िल्म है। फ़िल्म 2017 में प्रदर्शित हुई थी। सुभाशीष को 2017 के राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार में “विशेष उल्लेख” श्रेणी में नवाज़ा भी गया था।
इस कहानी का केन्द्रीय पात्र है राजीव, जो दयाशंकर का अधेड़ उम्र का बेटा है। छोटे शहर के मध्यम-वर्गीय परिवार में एक औसत नौकरी करने वाला ऐसा व्यक्ति, जो परंपराओं के प्रति कोई गहरी आस्था तो नहीं रखता लेकिन उन पर सवाल करना उसकी फ़ितरत नहीं है। बल्कि चुपचाप उनका पालन करने में उसे परेशानियाँ आती हैं तब भी वह कर्तव्ययबोध के चलते उनका निबाह करता चला जाता है। आधुनिकता और परंपरा में फंसी 60-70 के दशक में पैदा हुई पीढ़ी की नुमाइंदगी करता है राजीव का किरदार। आप अपने आस-पास, या स्वयं में इस किरदार की उलझनों को आसानी से देख सकते हैं।
यूं तो कहानी मौत के इंतज़ार की कहानी है, जहाँ दयाशंकर सहित सभी इस अवश्यंभावी मौत के लिए अपने और अपने आसपास के लोगों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन जिस खूबी से इस विषय को दिखाया गया है, कि फ़िल्म आपको लगातार बांधे रखती है। कई जगह पर हास्य का सहारा भी लिया गया है, जो बेहद ही संवेदनशीलता के साथ और आम ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़ा हुआ महसूस होता है। आम तौर पर परदे पर कहानी के विभिन्न रंगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नाटकीयता का सहारा लिया जाता है, लेकिन इस तरह के विषय जिसका ज़िक्र ही आपका ध्यान भंग कर सकता है उसमें सहजता और संतुलन ही विषय को दर्शाने का सही तरीका है।
एक दृश्य में राजीव की पत्नी लता, रात को चेहरे पर क्रीम लगाते हुए पूछती है, “कितने दिन लगेंगे?”, जिसके जवाब में राजीव कहता है, “मुझे क्या पता? गला दबा दूँ क्या?” इस दृश्य से राजीव की इस पूरे प्रकरण के प्रति, शुरुआती मनोदशा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पिता से परेशान और अपने सरोकारों में फंसा व्यक्ति। एक बेहद प्रभावशाली और प्रतीकात्मक दृश्य में हम, साझा टैक्सी में सफ़र करते हुए राजीव को बीच में फंसा, ऊँघता हुआ देख सकते हैं।
फ़िल्म में बनारस एक अहम किरदार है। हिन्दू धर्म की मान्यताओं में काशी का विशेष स्थान है। जन्म के बाद मुंडन से लेकर मृत्यु के बाद कर्म-कांड तक के लिए काशी और गंगा का खास महत्व है। अपने पिता की मृत्यु के इंतज़ार के साथ और उन्हे न छोड़ पाने की अपनी खीज को बहुत ही चतुराई के साथ बनारस की पृष्ठभूमि में दर्शाया गया है। दायित्वों और कर्तव्यों के बीच फंसे राजीव की मनोदशा और उसके संतुलन ढूँढने की उसकी कवायद, बनारस के विभिन्न दृश्यों के साथ प्रतीकात्मक तरीके से साथ फिल्माई गयी है। कहानी की शुरुआत में हरिशचन्द्र घाट पर राजीव का घूमना और उसके चश्मे में जलती चिताओं के प्रतिबिंब से लेकर, गंगा आरती के वक़्त उसके चश्मे में आरती के दीपों के प्रतिबिंब तक कहानी के कई मोड़, प्रभावशाली मोटीफ के जरिए हमारे सामने आते हैं। ताजदार जुनैद का संगीत भी फिल्म की सेटिंग के साथ पूरी तरह मेल खाता है।
सुभाशीष ने रीति रिवाजों के पाखंड और निरर्थकता की ओर भी इंगित किया है, लेकिन इसे कहानी का मुख्य बिन्दु नहीं बताया गया है। इसी प्रकार मौत की प्रक्रिया और आत्मा-परमात्मा का मिलन, मोक्ष इत्यादि का भी ज़िक्र है, लेकिन उसे भी नेपथ्य में ही उद्धृत किया गया है। कहानी का उद्देश्य धार्मिक कुरीतियों को उजागर करना नहीं है, न ही जीवन और मृत्यु के चक्र के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर टिप्पणी करना है। कहानी का फ़ोकस है मृत्यु की समीपता और स्वीकार्य के साथ आने वाले रिश्तों की बुनावट के फेर-बदल और जीवन-दृष्टि का विस्तार। और फ़िल्म इस फ़ोकस को लगातार बनाए रखती है।
फ़िल्म में वयोवृद्ध दयाशंकर की भूमिका में ललित बहल ने प्रभावशाली अभिनय किया है। अन्य कलाकारों में गीतांजलि कुलकर्णी, लता की भूमिका में, पालोमी घोष, राजीव की बेटी सुनीता की भूमिका में और अनिल रस्तोगी, मुक्ति-भवन के प्रबंधक मिश्रा’जी की भूमिका में बिल्कुल फिट बैठते हैं और सशक्त अदायगी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो कलाकार गहरी छाप छोड़ जाता है, वह है, राजीव की भूमिका में आदिल हुसैन की प्रस्तुति । आदिल हुसैन ने पात्र के हर उतार-चड़ाव को अभिनय की सूक्ष्म बारीकियों के साथ इस प्रकार अदा किया है, कि आप पात्र से जुड़े बिना नहीं रह पाते।
छोटी-छोटी बातें, जैसे घाट पर कपाल-भाति करना, सारे रहवासियों का टीवी पर सीरीअल देखना, भांग वाली मलाइयो खाना, राजीव का अपनी पत्नी से खाने को स्वादिष्ट बनाने के उपाय पूछना; ये सारी बातें, आम जीवन से निकाली गई हैं, लेकिन पात्रों की यात्रा को दर्शाने में अहम भूमिका निभाती हैं।
बड़ी सूक्ष्मता से काफी सारी बातों को छुआ गया है; मसलन, गंगा के सफ़ाई के विषय में कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक दृश्य में जब दयाशंकर को लगता है कि अंत निकट है तो वो राजीव से कहते हैं गंगाजल ला दो। जब राजीव गंगा तट से गंगाजल भर रहा है, तो वहीं बगल में एक व्यक्ति कपड़े धो रहा होता है।
एक दृश्य में जब दयाशंकर की तबीयत खराब होती है और उन्हे महसूस होता है कि उनका अंत निकट है, तो मुक्ति भवन के निवासी और भजन मंडली उनके गिर्द इकट्ठे होकर भजन गाती है। इस बीच दयाशंकर कहते हैं, कि थोड़ा सुर में गाओ। इस प्रकार से जीवन की विद्रूपताओं और दुखद परिस्थितियों में सहज हास्य के कई नमूने आप देख सकते हैं। इनका उद्देश हमेशा आपको हँसाना नहीं है, बल्कि ये जाताना है कि जीवन के रंग पल-पल बदलते हैं। अगर आप फ़िल्म देखें तो दयाशंकर और राजीव के बीच “कंगारू” संवाद और राजीव और सुनीता के बीच दयाशंकर का लिखा मृत्यु-संदेश पढ़ने के दृश्यों को देखें और महसूस करें कि किस तरह आम ज़िंदगी के आम से दिखने वाले दृश्य, रिश्तों को किस खूबसूरती से परिवर्तित और परिभाषित करते हैं।
अंतिम दृश्य में मुक्ति मिलने पर किया जाने वाला नृत्य अपने साथ इतनी सारी भावनाएँ लेकर आता है कि आप उनसे सराबोर हुए बिना नहीं रह पाते। अक्सर हम अपनी मृत्यु को देखना भूल जाते हैं। लेकिन हमें अचानक इसका भान तब होता है जब हमारे आसपास मृत्यु घटित होती है। ओशो की बात से ही अंत करता हूँ , “ मृत्यु कोई ऐसी बात नहीं है कि भविष्य में घटित होगी, इसीलिए हम उसे क्यों सोचें। मृत्यु प्रतिपल घटित हो रही है, पूर्ण भविष्य में होगी। यानि इस वक़्त भी हम मर रहे हैं। असल में जन्म से ही शुरू हो जाती है, इसलिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है।”
इस बार को समझ कर अगर हम जिन रिश्तों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हे सुलझाएँ और मृत्यु जो प्रतिपल हो रही है, उसके अंतिम पड़ाव का इंतज़ार न करें, तो आपका निवास ही आपका मुक्ति-भवन बन सकता है।
“मुक्ति भवन” को आप हॉट-स्टार पर यहाँ देख सकते हैं https://www.hotstar.com/in/movies/mukti-bhavan/1770016118/watch
~ मनीष कुमार गुप्ता






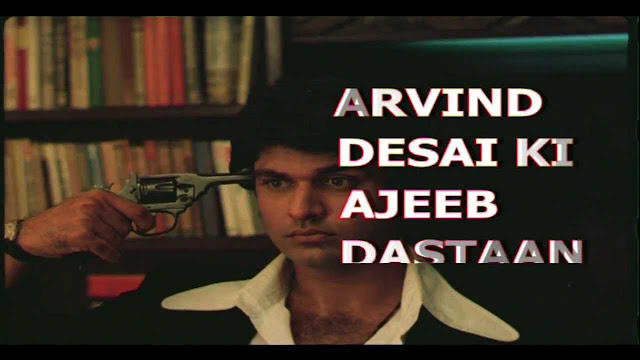
बहुत ही बढ़िया विषय हैं मृत्यु। इस पर कई व्याख्यान है और फ़िल्में हैं। स्वयं भी इस पर कई बार सोचते हैं। ज़िन्दगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र। यह गीत भी इस गंभीर विषय को बड़ी सरलता से चंद शब्दों में समेट लेता है। फ़िल्म देखने वाली लिस्ट में जोड़ ली है।
ReplyDelete🙏
Delete